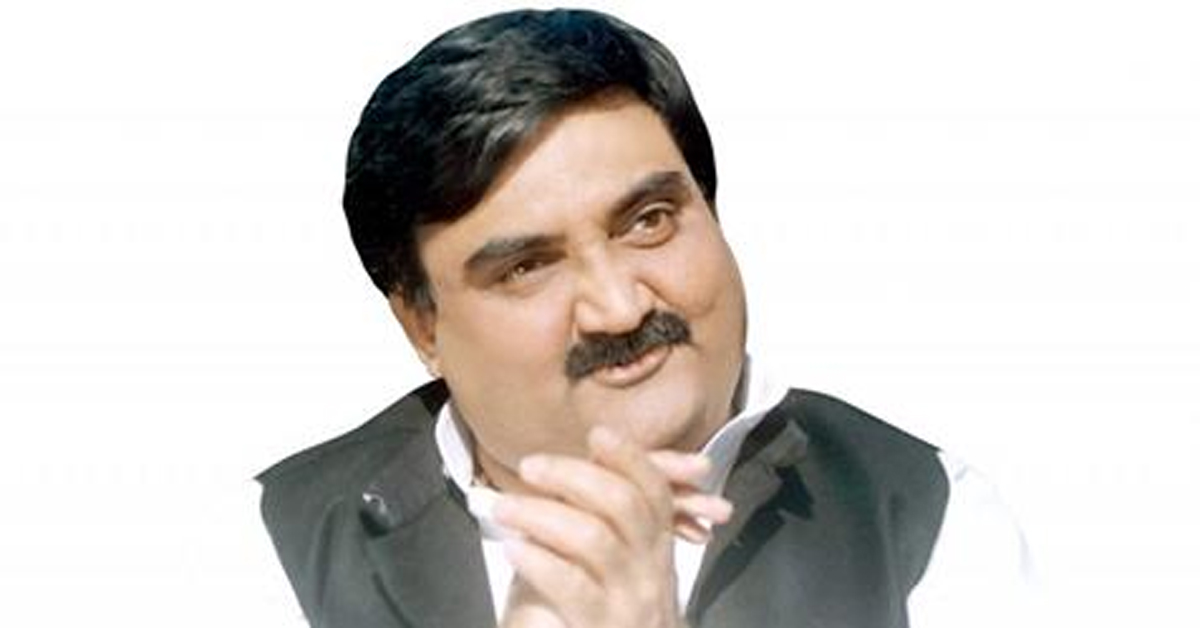सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की यह चिन्ता कहीं न कहीं हमारी समूची लोकतान्त्रिक व्यवस्था को सचेत करती है कि संविधान के दायरे से बाहर जाकर यदि हमने अपनी न्याय प्रणाली के प्रति नुक्ताचीनी का रुख अख्तियार किया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और हम अराजकता की तरफ बढ़ सकते हैं। संविधान दिवस (26 नवम्बर) के दिन इस प्रकार के विचार व्यक्त करके देश के प्रधान न्यायाधीश ने आगाह किया है कि भारत की लोकतान्त्रिक प्रणाली में ‘संविधान का संयम’ ही इसे कानून से चलने वाला राज बनाता है। यह समस्या इसलिए पैदा हो रही है कि कुछ तत्वों ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की समीक्षा करने के स्थान पर उनकी कटु आलोचना करनी शुरू कर दी है। सबसे पहले यह समझा जाना चाहिए कि भारत की संसदीय लोकतान्त्रिक राजनैतिक प्रणाली में बहुमत के शासन की व्यवस्था तो है, परन्तु उसकी कार्यप्रणाली की सीमाएं संविधान में ही निहित हैं।
हमारे संविधान निर्माताओं ने जो प्रणाली हमें सौंपी है उसमें संसद से लेकर अन्य चुने हुए सदनों मंे सरकारों का गठन राजनैतिक बहुमत के आधार पर ही होता है मगर यह अल्पमत में रहे किसी एक व्यक्ति के भी मौलिक व संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। बहुमत के आधार पर कोई भी समुदाय या राजनैतिक दल सामाजिक संरचना से लेकर इसके समावेशी वैविध्यपूर्ण चरित्र को अपनी मनमर्जी के माफिक किसी दूसरे वर्ग को न तो व्यथित कर सकता है और न ही उसे अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर सकता है। इसकी बुनियाद संसदीय लोकतन्त्र अपनाते हुए संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस प्रकार डाली कि बहुमत के शासन को संविधान के शासन के अधीनस्थ बनाया और प्रत्येक सत्ता प्रतिष्ठान को अपने अधिकारों के लिए केवल संविधान का ही मोहताज बनाया।
अतः मन्त्री से लेकर राष्ट्रपति तक को अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए संविधान पर ही निर्भर करना पड़ता है और इसकी सीमा पार करते ही उसका कृत्य संविधान के सख्त घेरे में आ जाता है। संविधान की व्याख्या करने के लिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व भी इस प्रकार निर्धारित है कि इसमें संजीदा मुकदमों का फैसला विद्वान न्यायाधीशों की पीठ बहुमत से करती है। अतः किसी भी न्यायिक पीठ द्वारा बहुमत से दिये गये फैसले को कोसा जाना संविधान का अपमान करने के अलावा कुछ और नहीं कहा जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को बदलने का अधिकार संसद के पास भी नहीं है मगर उसे यह अधिकार है कि वह उस कानून में बदलाव कर दे जिसकी रूह से सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला दिया है। इसके लिए उसे संविधान संशोधन करना होता है हालांकि संविधान संशोधन पूरी तरह राजनैतिक प्रक्रिया होती है मगर इसमें संविधान के बुनियादी ढांचे मंे बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रत्येक नागरिक के जीवन जीने की स्वतन्त्रता से लेकर धार्मिक, वैचारिक (अहिंसक) अधिकार होते हैं।
अतः बहुमत के विचार या धार्मिक मान्यता के विरुद्ध यदि एक व्यक्ति भी अपनी पृथक धारणा या विचार रखता है तो संविधान उसे पूरा संरक्षण देता है और सिद्ध करता है कि बहुमत के शासन का मतलब क्रूरता से किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी मर्जी के माफिक चलाने से नहीं है। यही वजह है कि हमारा संविधान आस्तिक से लेकर नास्तिक तक को अपना जीवन अपनी तरह से जीने की पूरी स्वतन्त्रता इस प्रकार देता है कि उसके कृत्य से किसी दूसरे को न कोई नुकसान पहुंचे और न कष्ट हो परन्तु अफसोस इस बात का है कि आज देश में बहुमत का तर्क देकर कुछ तत्व अपनी मर्जी के मुताबिक दूसरों को चलने के लिए मजबूर करते हैं और अपनी मान्यताएं उन पर लादना चाहते हैं। बल्कि इसके चलते न केवल सामाजिक हिंसा का खतरा इस प्रकार खड़ा होता है कि बहुमत का खौफ अल्पमत में रहने वाले लोगों के मौलिक व संवैधानिक अधिकारों का हनन करने लगता है मगर इसकी इजाजत घोषित तौर पर भारत का संविधान किसी को नहीं देता और बहुमत के शासन की व्यावहारिक व्याख्या करते हुए स्पष्ट करता है कि कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति बराबर है मगर खतरा यह बढ़ता जा रहा है कि जिस तरह कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को बहुमत की इच्छा की तराजू पर रखकर तोलने की धृष्टता कर रहे हैं उससे उनकी वह खिसियाहट प्रकट हो रही है जो बहुमत की राजनैतिक प्रणाली की व्यवस्था में संविधान के शासन की है।
यह सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है कि वह संवैधानिक दृष्टि से किसी भी मुकदमे की सुनवाई का वरीयता क्रम तय करे। उसके इस अधिकार की आलोचना का अर्थ है कि हम अपनी उस न्यायप्रणाली की विश्वसनीयता पर सन्देह कर रहे हैं जिसका सम्बन्ध केवल संविधान के प्रावधानों से है और ये प्रावधान आजादी के समय हमारे संविधान निर्माताओं ने तब बनाये थे जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी बची-खुची भौतिक सम्पत्ति के भी लुट-पिट जाने के बाद भारत बंटवारे की मजहबी उन्मादी विभीषिका से गुजर रहा था। अतः आज के नौसिखियों में इतनी कूव्वत नहीं हो सकती कि वे उस दौर की अंग्रेजों की साम्राज्यवादी सत्ता को हिलाने वाली पीढ़ी की दूरदृष्टि को भारत की बुनियादी बुनावट के मुद्दे पर चुनौती दे सकें और शेखी बघार सकें कि हमारी न्यायप्रणाली जनता की भावनाओं का संज्ञान नहीं ले रही है। दरअसल इस प्रकार का विचार ही स्वयं को संविधान से ऊपर मानते हुए व्यवहार करने का मार्ग प्रशस्त करता है जिसका असर बहुआयामी होता है।
यह नागरिकों द्वारा ही अपने विरोधी विचार रखने वाले दूसरे नागरिकों पर जुल्म करने की हिमायत में आकर इस प्रकार खड़ा हो जाता है कि समूचे देश की सामाजिक संरचना खतरे में आ जाती है और इसके खतरे में आते ही राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए यह बेवजह नहीं था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक के भारतीय राज्यों के लोगों को जिस देश भारत में बांधा उसे ‘राज्यों के संघ’(यूनियन आफ इंडिया) का नाम देते हुए प्रत्येक राज्य को विशिष्ट अधिकार देकर अपनी-अपनी भौगोलिक, सामाजिक व शैक्षणिक परिस्थितियों के अनुसार अपने लोगों के विकास के लिए अपने विवेक से निर्णय लेने का अधिकार दिया। इसका मन्तव्य यही था कि किसी भी सूरत में बहुमत के क्रूर मत का डर खुद को अल्पमत में समझने वाले किसी भी राज्य से लेकर व्यक्ति तक में घर न कर सके। अतः देश में विपक्ष के नेता श्री शरद यादव से लेकर अन्य दलों के नेता जो संविधान बचाओ आन्दोलन चला रहे हैं वह निरर्थक नहीं है। उसके पीछे भारत की एकता को मजबूत रखने की ख्वाइश इस तरह छिपी हुई है कि अम्बेडकर के संविधान को किसी भी सूरत में फौरी सियासी तहरीरों के तीरों से बचाया जा सके।