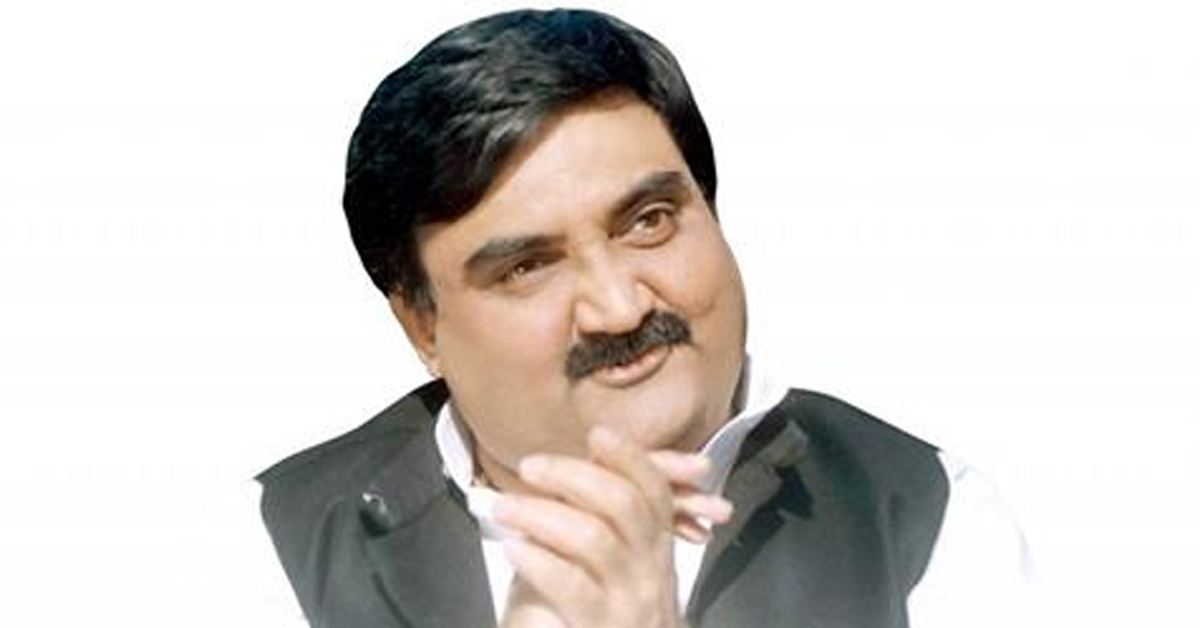मेरे हम उम्र लोग जरा सोचें कि क्या हम सबने बचपन में अपने कंधों पर स्कूली बस्ते का भारी भरकम बोझ महसूस किया था? हम तो मुस्कुराते हुए, हल्के बस्ते को घुमाते भागते घर लौटा करते थे। स्कूल से लौटते ही घर के आंगन में बस्ता पटक कर खेलने चले जाते थे। बिना किसी तनाव के जिन्दगी का आनंद लेते थे। देखते ही देखते बस्तों का वजन बढ़ने लगा और उसके बोझ से बचपन सिसकने लगा। अब तो स्कूल जाने के लिए बसें हैं, निजी वाहन हैं, अभिभावकों के पास अपनी गाडि़यां हैं, फिर गेट के स्कूल से लेकर कक्षा तक बस्ते का बोझ लेकर चल पाना मुश्किल हो गया है। बदलते दौर में बस्तों का भारी भरकम बोझ तो अभिभावक ही उठाते हैं। यह सही है कि शिक्षा के तरीकों में बदलाव आया है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारी बस्तों से शिक्षा सुधर गई है या आज के बच्चे ज्यादा अच्छी शिक्षा पा रहे हैं।
आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवार वाले तो अपने बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा का बोझ सहना ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे परिवारों के बच्चों को आप कंधों पर भारी बस्ता टांगे सड़कों पर भागते, हांफते देख सकते हैं। स्कूली बच्चों पर बोझ कम करने की चर्चा कई वर्षों से होती आई है लेकिन केन्द्र सरकार ने कदम अब उठाए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि पहली और दूसरी के छात्रों को होमवर्क न दिया जाए आैर उनके बस्तों का वजन भी डेढ़ किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मंत्रालय ने पहली से लेकर दसवीं क्लास तक के बच्चों के बस्ते का वजन भी तय कर दिया है।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि पहली और दूसरी क्लास के बच्चों के लिए भाषा आैर गणित के अलावा कोई दूसरा विषय तय नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी से पांचवीं तक एनसीईआरटी द्वारा तय भाषा, गणित और पर्यावरण विज्ञान के अलावा दूसरे विषय नहीं पढ़ाने चाहिएं। मानव संसाधन मंत्रालय का यह कदम सराहनीय है। छह वर्ष पहले 2012 में बच्चों पर भारी बोझ को लेकर एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले थे। सर्वे के अनुसार बस्ते के बढ़ते बोझ के कारण पांच से बारह वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों में अधिकांश पीठ के दर्द से पीड़ित थे। बोझ के चलते उनकी हड्डियों और उनके शरीर के विकास पर विपरीत असर पड़ने की आशंका जाहिर की गई थी। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तो ठीक तरीके से बैठ भी नहीं सकते थे। उन्हें पीठ के दर्द, कंधे में दर्द तथा रीढ़ की हड्डी से संबंधित कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई थीं।
बस्तों के बढ़ते बोझ से बच्चों का शारीरिक तनाव से प्रभावित होना स्वाभाविक है। जब से स्कूलों में शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ तब से बच्चों का तनाव बढ़ता गया। देश के स्कूलों में अलग-अलग शिक्षा प्रणालियां प्रचलित हैं। स्कूली शिक्षा को दिनोंदिन कम बोझिल और व्यावहारिक बनाने के प्रयास किए जाते रहे हैं, आैर आगे भी किए जाते रहेंगे। एक दिन में छह-सात पीरियड लगाए जाने लगे, स्वाभाविक है कि सात पीरियड की पुस्तकें और साथ में खेलों का सामान, बोझ तो बढ़ना ही था। ऐसा भी नहीं है कि स्कूली बच्चों पर बस्तों का बोझ चर्चा का विषय नहीं बना हो। दशकों पहले आर.के. नारायण ने अपने स्तर पर इस बोझ को लेकर संसद में यह मामला उठाया था, परन्तु तब भी राजनीतिक दल आम राय नहीं बना सके थे।
बच्चों पर बोझ बढ़ाने के लिए अभिभावक भी कम जिम्मेदार नहीं। दरअसल कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में अभिभावक अपने बच्चों को पैसे उगलने वाला एटीएम बनाना चाहते हैं और वे बचपन में ही बच्चे पर अपनी महत्वाकांक्षाओं का दबाव डालना शुरू कर देते हैं। स्कूल से आते ही बच्चों को ट्यूशन पर भेज दिया जाता है। घर लौटते ही बच्चे टी.वी. देखने लग जाते हैं या फिर कम्प्यूटर पर बैठ जाते हैं। खेल के मैदान में जाने की फुर्सत किसे है।
आपाधापी, भागमभाग के चक्र ने सब कुछ बदल दिया है। एकाकी परिवारों के चलते दादी-दादा, नानी-नाना तथा अन्य परिवारजनों के स्नेही सान्निध्य से वंचित हुए बच्चे कम्प्यूटर पर खेलने और ऊल-जुलूल कार्यक्रम देखने को विवश हैं। अब तो दो वर्ष के बच्चों को प्ले स्कूल के नाम पर स्कूल भेज दिया जाता है। मोबाइल और आधुनिक उपकरणों के चलते बच्चे उम्र से पहले परिपक्व हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अभिभावकों के पास समय ही नहीं बचा। शैक्षिक व्यवस्था में बार-बार कहा गया कि बस्तों का बोझ कम किया जाए परन्तु व्यवहार में स्थिति नहीं बदली। स्कूल प्रबंधकों ने, अभिभावकों को तो पढ़ा-लिखा नागरिक चाहिए, यह देखने की आवश्यकता ही नहीं समझी कि भविष्य का नागरिक कैसे पढ़ रहा है, कैसे जी रहा है? बचपन की नाजुक उम्र में ही पीठ पर बोझ डाल हांक दिया स्कूल की ओर जहां बकरियों की तरह बच्चे भर दिए जाते हैं।
एक बच्चे का सम्पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वह स्वछन्द वातावरण में पले-बढ़े। बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी है प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण वातावरण, जहां वे पानी की कलकल को सुनें, पक्षियों की चहचहाट को समझें। बोझिल वातावरण में आज के बच्चे पर माता-पिता की आकांक्षाओं का बोझ भी है और उस पर अभिभावकों की सामाजिक प्रतिष्ठा का बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इन सब को उसका बालपन संभाल नहीं पाता और वह आगे बढ़ने की अपेक्षा परीक्षा में फेल होने के डर से मौत को गले लगा लेते हैं। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं। बच्चों के विकास के लिए सार्थक कदम उठाने जरूरी हैं। नौनिहालों को इनका बचपन लौटाना ही होगा।