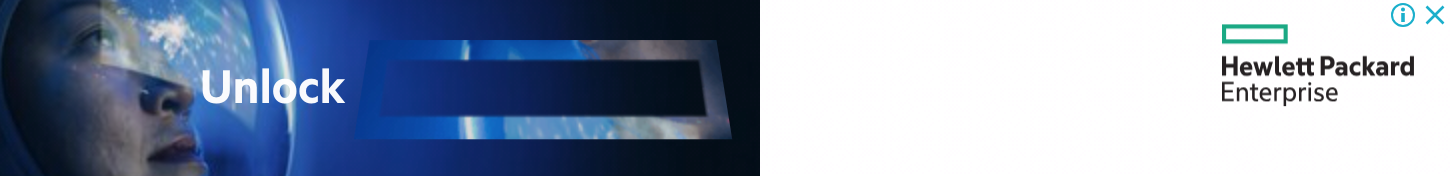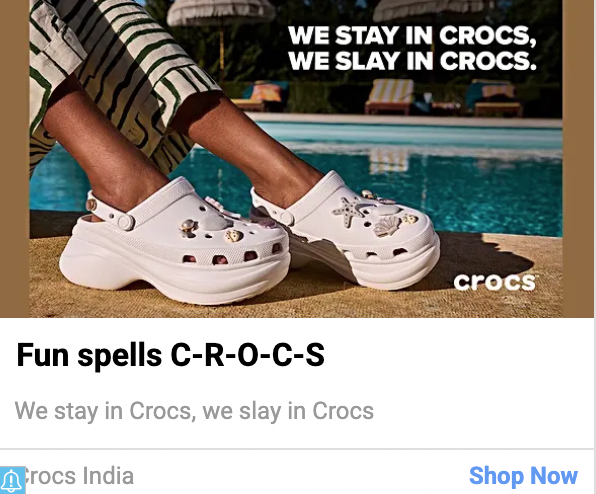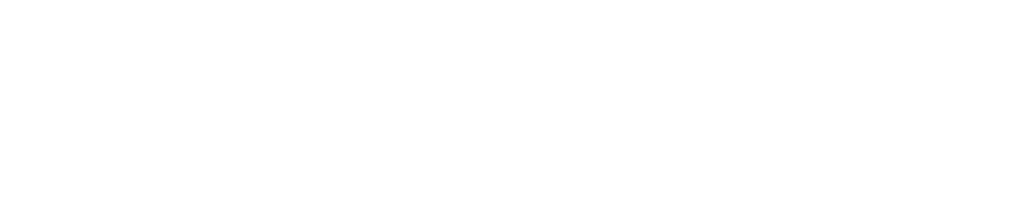तेलंगाना के मुख्यमन्त्री के.सी. राव ने राज्य विधानसभा को आठ महीने पूर्व ही भंग करने की सिफारिश करके एेसा राजनीतिक दांव खेलने की कोशिश की है जिससे उनके दोनों हाथों में लड्डू रहें। उनकी सरकार का कार्यकाल अगले वर्ष मई महीने तक था और वह तब तक आराम से मुख्यमन्त्री बने रह सकते थे मगर अगले साल मई में ही लोकसभा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है अतः केन्द्र की मोदी सरकार को भी इससे पूर्व ही लोकसभा भंग करके नए चुनाव कराने की सिफारिश करनी पड़ेगी। एेसी सूरत में लोकसभा के साथ ही तेलंगाना विधानसभा के चुनाव भी होते लेकिन तेलंगाना के पितृ राज्य समझे जाने वाले आंध्र प्रदेश में भी अगले साल लोकसभा के साथ ही चुनाव होने हैं और पूर्व के राज्य ओडिशा की भी यही स्थिति है। इसके साथ ही चार राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान व मिजोरम की विधानसभाओं का कार्यकाल इसी वर्ष दिसम्बर में समाप्त हो रहा है अतः इन चार राज्यों में इससे पूर्व नवम्बर महीने में ही चुनाव होने तय हैं।
अब चुनाव आयोग को पांचवें राज्य तेलंगाना का चुनाव भी इन चारों राज्यों के साथ कराना पड़ेगा लेकिन मूल राजनीितक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि श्री राव ने जल्दी चुनाव कराने का जोखिम क्यों लिया? क्या उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि यदि उनके राज्य में चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ हुए तो उनकी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को नुकसान हो सकता है और राज्य चुनाव के मुद्दे लोकसभा के राष्ट्रीय चुनावी मुद्दों के साये में आकर हल्के पड़ जाएंगे ? यदि उन्हें इस बात का डर है तो फिर पड़ोसी राज्य आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री चन्द्रबाबू नायडू क्यों निडर होकर सुनिश्चित समय पर ही चुनाव के लिए अड़े हुए हैं। दरअसल श्री राव के फैसले में अपने ऊपर ही अविश्वास का भाव छिपा हुआ है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों। दोनों चुनावों के मुद्दे अलग-अलग ही रहेंगे। भारत के मतदाताओं में इतनी बुद्धिमत्ता शुरू से ही रही है कि वे राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के गठन के लिए जब मतदान करते हैं तो यह सोचकर ही करते हैं कि उनके लिए राज्य में कौन सी पार्टी बेहतर साबित होगी और केन्द्र में कौन सी।
इसके एक नहीं अनेकों प्रमाण हैं, 1976 तक लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे मगर ओडिशा व केरल एेसे राज्य रहे जहां 1967 से पहले के हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी को अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी सफलता नहीं मिल पाती थी लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण 1971 के लोकसभा चुनावों के बाद हुए दिल्ली नगर निगम के चुनाव कहे जा सकते हैं। लोकसभा चुनावों में स्व. इंदिरा गांधी की नई कांग्रेस को तब दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर अपार सफलता मिली थी मगर इसके महीने भर बाद ही हुए निगम चुनावों में उन्हीं मतदाताओं ने जनसंघ को बहुमत दिया था। निगम चुनावों के समय अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार करते समय जनसंघ के शीर्षस्थ नेता स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि दिल्ली वालो आपने हमें राष्ट्रीय राजनीति के काबिल तो नहीं समझा मगर अब हमारे हाथ में झाड़ू तो रहने दो जिससे हम दिल्ली की साफ- सफाई करने में आपकी मदद करें लेकिन ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं। संवैधानिक और कानूनी पहलू यह है कि श्री राव ने तेलंगाना विधानसभा में अपना पूर्ण और पक्का बहुमत होते हुए भी आठ महीने पहले ही विधानसभा भंग करा कर चुनाव आयोग के सामने चुनौती फैंक दी है कि वह अब चार राज्यों के साथ ही तेलंगाना के चुनाव भी कराए। विधानसभा के भंग होने के बाद अगले छह महीने के भीतर-भीतर इस सदन का दूसरा सत्र आहूत किया जाना चाहिए।
जिसे देखते हुए अगले वर्ष मार्च महीने से पहले नई विधानसभा हर हालत में गठित हो जानी चाहिए। इस सूरत में तेलंगाना विधानसभा के चुनाव संवैधानिकतः हर हालत में लोकसभा के चुनावों से पूर्व कराने पड़ेंगे क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल मई महीने में समाप्त होगा। यही वजह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओ.पी. रावत ने तेलंगाना के मुख्यमन्त्री के इस कदम को पूरी तरह ‘अनर्गल’ या असंगत बताया है। राजनीतिक लाभ की इच्छा में इस प्रकार के कदम जब उठाए जाते हैं तो उनका मन्तव्य जनहित किस प्रकार हो सकता है ? मगर श्री राव अपनी ‘डेढ़ ईंट’ की मंजिल बनाने के लिए शुरू से ही प्रसिद्ध रहे हैं। उनका एक हाथ कांग्रेस के साथ रहता है तो दूसरा भाजपा के साथ। वह कभी विपक्षी एकता की बातें करने लगते हैं तो कभी संसद में उनकी पार्टी के सांसद भाजपा के हक में खड़े हो जाते हैं। राज्य में उनकी पार्टी भी परिवारवाद का ही जीता-जागता नमूना कही जा सकती है जिसमें उनकी पुत्री से लेकर पुत्र तक का दबदबा है। लोकरंजक राजनीति वही कहलाई जाती है जिसमें साधारण वर्ग के लोगों का दबदबा सामने आता है मगर भारत में गजब की राजनीति हो रही है कि लगभग सभी क्षेत्रीय दलों में जमकर खानदानी राज चल रहा है और पार्टियां एेसे चल रही हैं जैसे कोई कदीमी परचून की दुकान हो। लोकतन्त्र में उस लोक (लोगों) को ताकत दी जाती है जिन्हें सामाजिक वर्जनाएं सत्ता में भागीदारी से दूर रखे रहती हैं…इन्हीं वर्गों के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक सशक्तीकरण का नाम लोकतन्त्र होता है जो किसी परिवार का मोहताज नहीं होता मगर क्या कयामत है कि लोकतन्त्र में ही नए-नए खानदानी रजवाड़े पनप रहे हैं।