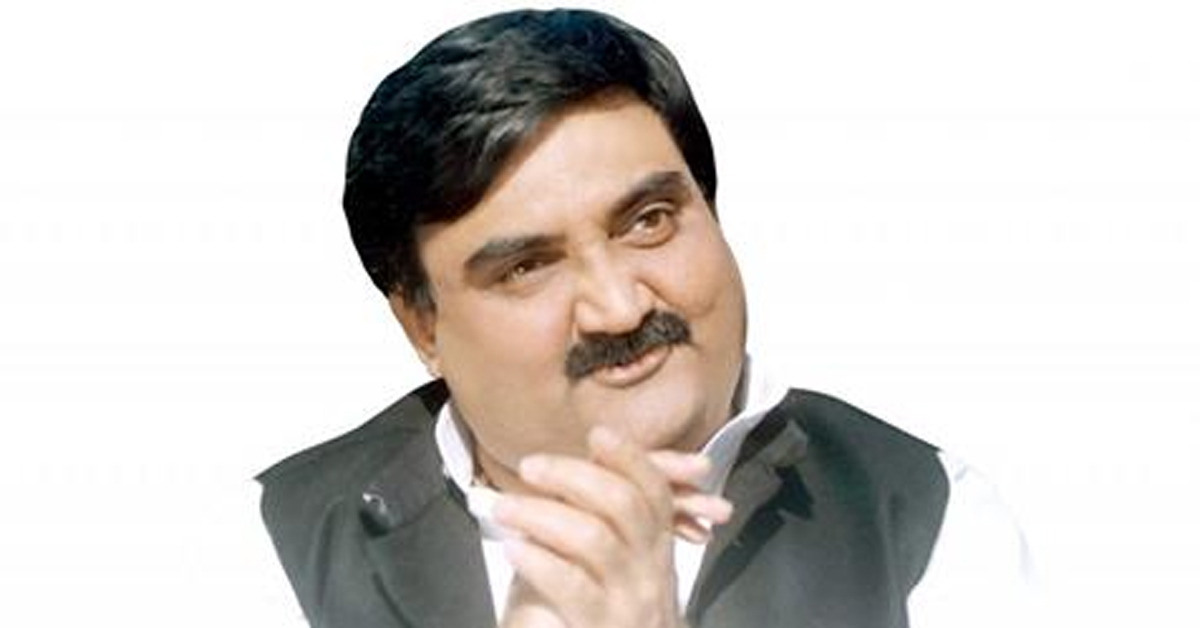यदि देश की सबसे बड़ी जांच एजैंसी सीबीआई के भीतर ही इसके उच्च अफसरों के बीच एक-दूसरे पर आरोप लगाने के साथ ही कानूनी कार्रवाई करने की हद तक बात जा सकती है तो निश्चित रूप से इसका अर्थ यही है कि इस संस्था का सस्ता राजनीतिकरण हो चुका है और इसकी विश्वसनीयता का संकट खड़ा होने वाला है मगर इसके लिए सीबीआई के सुविचारित ढांचे को दोष नहीं दिया जा सकता बल्कि इसका जिम्मा उस राजनीति का है जिसने इस संस्था को अपना ही एक अंग बनाने की भूल कर डाली है। यह प्रक्रिया पिछले कुछ सालों से ही नहीं चली है और न इसके लिए किसी एक सरकार को दोष दिया जा सकता है बल्कि इसके लिए पिछले तीस सालों से चल रही देश की अवसरवादी सत्ता लोभी राजनीति पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराई जा सकती है।
जब राजनीति सिद्धांतविहीन होकर सत्ता में आने भर की खातिर बेमेल गठजोड़ करती है तो वह लोकतन्त्र की उस पारदर्शिता, सादगी और शुचिता से समझौता करती है जो इस प्रणाली में शासन करने की मूल शर्त होती है। पिछले तीस सालों में इसी देश ने एेसे लोगों को सीबीआई की कमान के सबसे ऊंचे पायदान तक पर देखा है जिन पर स्वयं सीबीआई ने ही चार्जशीट दायर करके मुकद्दमे दर्ज किए हुए थे। तब राजनीति ने अपराध की भी नई परिभाषा गढ़ने में कोई हिचक नहीं दिखाई और कहा कि कथित जनांदोलनों के रोष की ज्वाला में मरने वाले लोगों का रंग सामान्य अपराध के क्रोध में मरने वाले लोगों के रंग से अलग होता है। एेेसे भी अवसर इन पिछले तीस सालों में आए जब देश के प्रधानमन्त्री को स्वयं संसद में आकर सफाई देनी पड़ी कि वह इस जांच एजैंसी की निष्पक्षता की गारंटी देते हैं।
यह भी बेसबब नहीं था कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को ‘पिंजरे में बन्द तोता’ तक बताते हुए इसकी कार्यप्रणाली पर अंगुली उठाई थी। जाहिर है न्यायालय की यह टिप्पणी इस संस्था को राजनीतिक रूप से कब्जे में किए जाने को लेकर ही थी। उस समय केन्द्र में डा. मनमोहन सिंह की सरकार थी और विपक्ष में बैठे हुए तब भाजपा के नेता श्री लालकृष्ण अडवानी फरमाया करते थे कि डा. मनमोहन सिंह की सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी संस्था ‘सीबीआई’ है जो इसे सत्ता में बनाए रखने के लिए विरोधियों को डराने के काम में लगी हुई है। समय बदला, सरकार बदली मगर आरोपों का चरित्र नहीं बदला, अर्थात सीबीआई की विश्वसनीयता जैसी थी वैसी ही रही। इस बीच यह विवाद भी गर्माया कि सीबीआई को एक स्वतन्त्र दर्जा दे दिया जाना चाहिए।
इसे राजनीतिक नियन्त्रण से मुक्त किया जाना चाहिए परन्तु यह मांग पूरी तरह उस अधकचरे सोच की परिचायक थी जिसमें लोकतन्त्र में संविधान के शासन को संसद की प्राथमिक जिम्मेदारी बनाने से छुटकारा पाने का प्रयास निहित था। किसी भी संसदीय लोकतन्त्र में कोई भी संस्था संसद से ऊपर नहीं हो सकती क्योंकि एेसा होते ही जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की सत्ता, साख और अधिकार आम जनता के नियन्त्रण से बाहर निकल कर संविधानेत्तर संगठन के नियन्त्रण में चले जाते हैं जिससे प्रत्यक्ष रूप से तानाशाही का रास्ता निकलता है। अतः भारत की कोई भी सरकार सीबीआई जैसी संस्था को बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती मगर इसका राजनीतिकरण भी नहीं कर सकती। इसी वजह से सीबीआई के प्रमुख की नियुक्ति के लिए जो नया फार्मूला हमने निकाला उसमें इस पद की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को काबिज रखने की गरज से नियुक्ति करने वाले मंडल में प्रधानमन्त्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया।
बहुमत से इस नियुक्ति का विधान करके हमने तय किया कि सीबीआई प्रमुख सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त रहें और अपना कार्य पूरी स्वतन्त्रता के साथ करते हुए अपने कर्तव्य को निभाएं परन्तु यह प्रयोग भी क्या सफल कहा जा सकता है? क्योंकि हालत यह हो रही है कि सीबीआई के दो प्रमुख निदेशक राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा एक-दूसरे के खिलाफ ही तलवारें खींचते नजर आ रहे हैं। ये दोनों अफसर एक-दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और एफआईआर सीबीआई ही दर्ज कर रही है। ये सारे मामले भ्रष्टाचार को लेकर ही दर्ज हो रहे हैं। इस मंजर पर सिवाय रोने के और क्या किया जा सकता है क्योंकि 1963 में भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने जब विशेष दिल्ली पुलिस कानून का विस्तार करते हुए सीबीआई का गठन किया था तो इसका उद्देश्य उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच करना था मगर आज हालत यह हो गई है कि इसके ऊंचे अफसर खुद ही एक-दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकद्दमे दर्ज करा रहे हैं! क्या असर डाला है राजनीति ने कि मुंसिफ ही मुजरिम की हालत में आ गया है। खुदा-या–खैर।