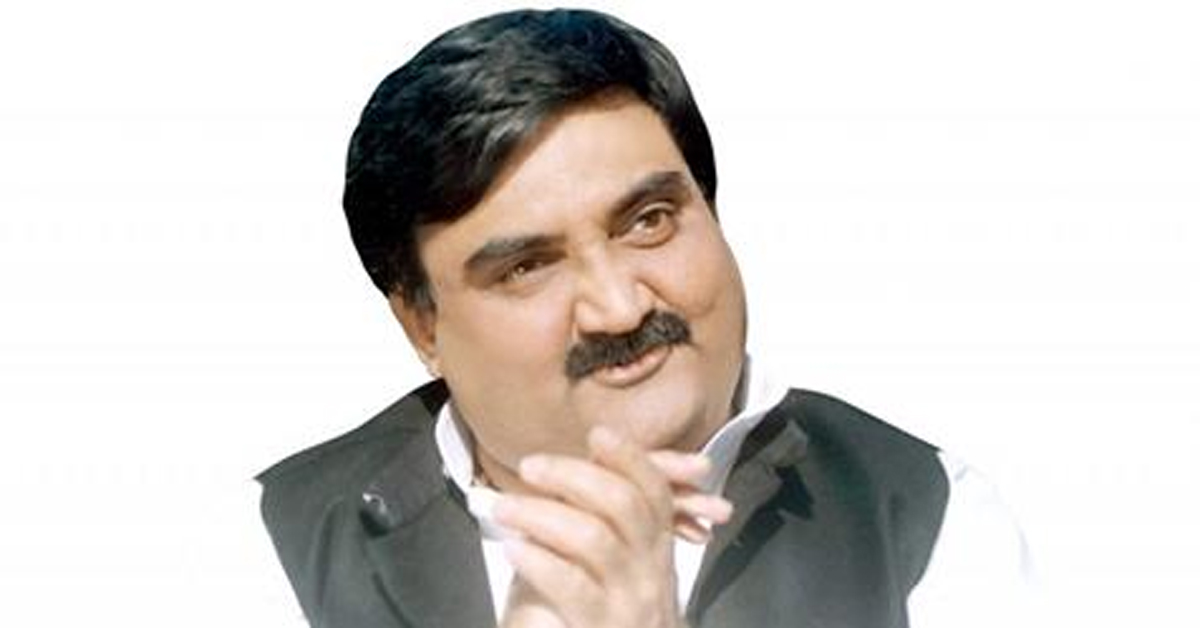वनवासियों को जंगल की जमीन खाली करने के अपने ही आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक से आदिवासी-वनवासी समाज को बड़ी राहत दी है। इस रोक से 10 लाख से ज्यादा आदिवासियों को बेदखली से बचा लिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की बैंच ने प्राकृतिक दुनिया के दावेदारों यानी आदिवासियों को अतिक्रमणकारी मान लिया था और 21 राज्यों को यह आदेश दिया था कि उन्हें जंगलों से बेदखल कर दिया जाए। इस पीठ ने यह फैसला किस आधार पर किया, इस पर सवाल उठने लगे थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नए तथ्यों के आलोक में अब पहले ही फैसले को पलटते हुए बेदखली के आदेश पर रोक लगा दी है। 2005 में संसद ने वन अधिकार कानून बनाया था।
यह स्वीकार किया गया था कि देश में 8.08 फीसदी आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक रूप से नाइन्साफी हुई है। ब्रिटिशकाल 1793 में स्थायी बंदोबस्ती शुरू होने के बाद से ही इन्हें बेदखली का सामना करना पड़ा है। कभी इन्हें वन्यजीवों की सेंचुरी और नेशनल पार्कों के लिए उजाड़ा गया। 187 जिले जो कि भारतीय सीमा के भीतर का 33.6 प्रतिशत क्षेत्र होता है। इन जिलों में 37 प्रतिशत क्षेत्र सुरक्षित वन हैं और 63 प्रतिशत घने जंगलों के इलाके माने जाते हैं। लाखों लोग वे हैं जो सदियों से जंगलों, पहाड़ों, तराई और वहां के मैदानी इलाकों में रहते चले आ रहे हैं। इन्हीं लोगों को आजादी मिलने के बाद भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है।
विडम्बना यह रही है कि हम अपने ही देश में अपने ही लोगों को उजाड़ते आ रहे हैं और इनके पुनर्वास की कोई ठोस व्यवस्था भी नहीं है। इस मामले का मानवीय पहलू इतना संजीदा है कि सुप्रीम कोर्ट को इन्हें बड़ी राहत देनी पड़ी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल जरूर उठाया कि राज्य सरकारें अब तक सोई क्यों रहीं? दरअसल राज्य सरकारें मानवीय पहलू को लगातार नजरंदाज कर रही हैं। संविधान में भी आदिवासियों के आदिम लक्षणों, भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट संस्कृति, बाहरी समुदाय के साथ सम्पर्क में संकोच और आर्थिक पिछड़ेपन को आधार मानकर देश की कल्याणकारी व्यवस्था में सुविधाओं से जोड़े जाने का प्रावधान भी है। इन्हें देश का मूल निवासी कहते हुए सरकार और संसद ने भी माना कि जंगलों पर पहला अधिकार आदिवासियों का है और इसी वजह से वनाधिकार नियम 2006 अस्तित्व में आया था।
यह कानून 31 दिसम्बर 2005 से पहले कम से कम तीन पीढ़ियों तक वनभूमि पर रहने वालों को भूमि अधिकार देने का प्रावधान करना है। दावों की जांच जिला कलैक्टर की अध्यक्षता वाली समिति और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाती है। इनके अधिकांश दावे खारिज कर दिए गए क्योंकि अनेक के पास जमीन का कोई दस्तावेज ही नहीं है। वह इस बात को प्रमाणित ही नहीं कर पाए कि वे सदियों से यहां रहते आए हैं। प्रशासनिक मशीनरी अपने कायदे-कानूनों से काम करती है। न्यायालय सबूत मांगता है। केन्द्र सरकार ने भी इनके पक्ष को मजबूती से नहीं रखा और राज्य सरकारों को इनकी समस्याओं का पता ही नहीं है।
आर्थिक उदारीकरण की नीतियां लागू होने के बाद यह शब्द उस दुनिया के लिए बन गया जिन्होंने अपने पांव तेजी से पसारे और जल, जंगल और जमीन पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। खनन कम्पनियां और अन्य कार्पोरेट सैक्टर ने देश के संसाधनों की लूट शुरू की। अवैध खनन और वन माफिया सक्रिय हो उठा। आदिवासियों को मूल से उजाड़ा जाने लगा। आर्थिक उदारीकरण समाज के उन हिस्सों के लिए कहा है, जिनके पास बोने, उगाने और खाने के लिए अपना श्रम और उसका उपयोग करने के लिए जमीन ही सब कुछ है। आदिवासियों की जमीन और उसके नीचे दबी प्राकृतिक सम्पदा और आसपास का वातावरण जैसी पूंजी सदियों से सुरक्षित है और संरक्षित रही है। आर्थिक उदारीकरण के पहले दौर में देखा गया कि मैदानी इलाकों में भूमि की लूट तो हुई ही, जंगलों की भूमि की भी लूट हुई।
ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन की छीना-झपटी अगर हुई तो वह भारत में हुई। जंगलों के ठेकेदारों और सरकारी नौकरशाहों ने कानूनों की आड़ लेकर आदिवासियों के खिलाफ दमन का सिलसिला बनाए रखा। देश में नक्सली समस्या के मूल में ही आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन से वंचित करना ही है। जंगलों के दावेदारों का फैसला करने वाले लोग हैं। देश में सामाजिक संगठन माने जाने वाले एनजीओ जंगलों में तैनात किए गए नौकरशाह, ब्रिटिशकाल के दौरान स्थायी बंदोबस्ती के वक्त मालिकाना हक पाने वाले जमींदार और थाना, कचहरी, जंगलों के दावेदारों की अपनी ग्रामसभाएं भी हैं। सामाजिक संगठनों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं की भूमिका भी संदेह के घेरे में रही है। कुछ एनजीओ तो कार्पोरेट घरानों के लिए काम करते दिखाई दे रहे हैं।
पर्यावरणविदों की चिन्ताओं की मार समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर हिस्सों को ही उठानी पड़ रही है। जंगलों में जानवरों के लिए संरक्षित जगह बनी है। बड़े-बड़े बांध बनाए गए, नेशनल पार्क बनाए गए लेकिन इन्सानों को उजाड़ा गया, उन्हें भूखे मरने को मजबूर किया गया। आज बड़े-बड़े मुद्दों पर जाने-माने वकील अदालतों में स्वयं खड़े हो जाते हैं और संविधान की व्याख्या कर बड़े-बड़े मुद्दों को चुनौती देते नजर आते हैं और लोकप्रियता हासिल करते हैं। अफसोस आदिवासियों के लिए कोई प्रतिष्ठित वकील खड़ा नहीं हुआ। आदिवासियों ने समाज, जंगल और प्रकृति के लिए हमेशा अन्याय सहा।
लम्बी लड़ाई लड़ने के बावजूद इन्हें मालिकाना हक क्यों नहीं मिला? आदिवासी तो वन, वनस्पतियों की रक्षा करते आए हैं लिहाजा सरकार को इन परिवारों के प्रति नरम रवैया अपनाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय को भी इनकी बेदखली के साथ-साथ इनके पुनर्वास की बात करनी चाहिए। राज्य सरकारों को भी इन्हें बसाने के लिए जमीन के पट्टे देने चाहिए। अगर अपने ही देश के लोग पराये हो जाएंगे तो समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है।