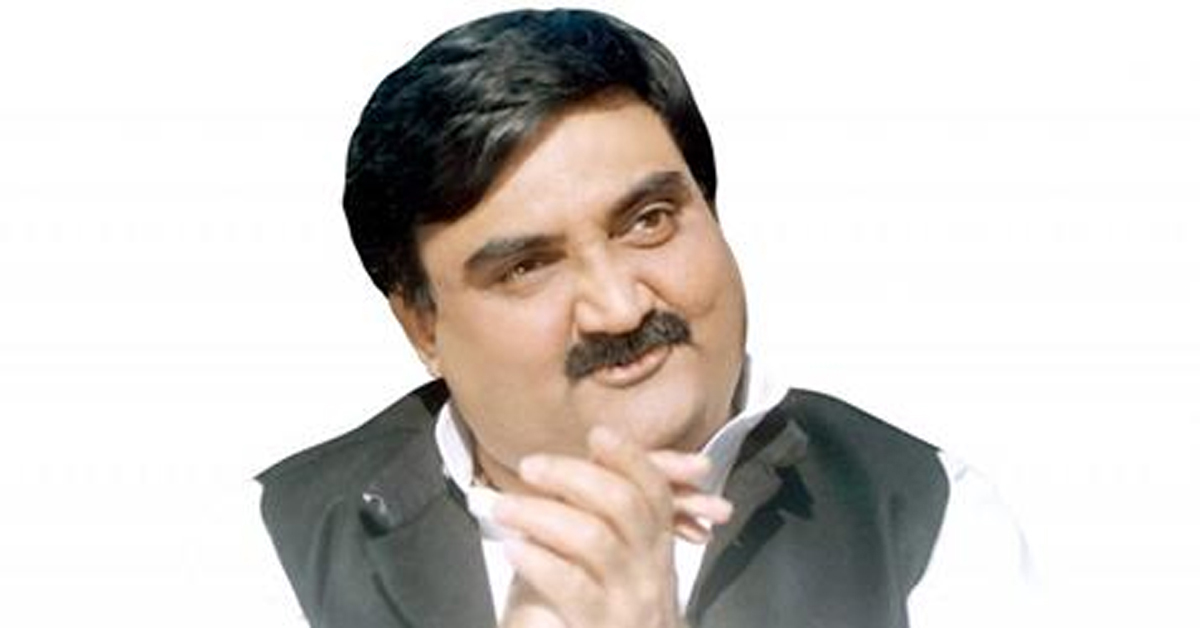बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में ‘चमकी’ बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या जिस तरह लगातार बढ़कर दोहरे शतक की तरफ पहुंच रही है उससे केवल इसी राज्य की नहीं बल्कि समूचे भारत की स्वास्थ्य व चिकित्सा व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। विशेष रूप से सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र का। स्वास्थ्य क्षेत्र में जो ‘मरघट’ की सी हालत है वह आम हिन्दोस्तानी की व्यथा को बखान कर रही है। पिछले दिनों प. बंगाल में जिस तरह डाक्टरों की हड़ताल सुरक्षा देने के नाम पर चली उसका सम्बन्ध भी परोक्ष रूप से इसी समस्या से जाकर जुड़ता था। हालांकि इस राज्य में भयावहता का वह स्वरूप प्रकट नहीं हुआ था जो बिहार में हुआ है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि प. बंगाल में जहां प्रत्येक दस हजार लोगों पर एक चिकित्सक का औसत है वहीं बिहार में यह 28 हजार लोगों पर एक डाक्टर का है किन्तु चिन्ता की बात बिहार के सन्दर्भ में सबसे ज्यादा यह है कि पिछले पांच साल से ‘चमकी’ बुखार गर्मियों के मौसम का ‘बालभक्षी’ बना हुआ है और राज्य सरकार इस पर सामान्य गति से काम कर रही है।
चमकी बुखार को ‘क्रूर जापानी बुखार’ की ऐसी किस्म माना जा रहा है जिसका कोई टीका अभी तक ईजाद नहीं हो पाया है और इस बारे में लगातार चिकित्सीय प्रयोग व खोज हो रही है। संसद के दोनों सदनों में भी यह मसला खूब गर्मागर्मी से उठ चुका है। लोकसभा में भाजपा सांसद श्री जगदम्बिका पाल ने इस बुखार के अंतर्राष्ट्रीय प्रकोप का विवरण प्रस्तुत करके यह तक बता दिया कि कम्बोडिया जैसे देश में इस पर काबू पा लिया गया है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मन्त्री डा. हर्षवर्धन ने अपने पिछले कार्यकाल में किये गये कार्यों का ब्यौरा भी मीडिया में खूब रखा मगर सवाल यह है कि पांच सालों में इस मोर्चे पर क्या उपलब्धि हासिल की गई? इसी सन्दर्भ में भाजपा के बिहार से लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने गर्मियों के मीठे फल ‘लीची’ के साथ इस बुखार का सम्बन्ध जोड़े जाने पर ऐसी चिन्ता प्रकट की जिसकी तरफ चाहे-अनचाहे ध्यान देना ही होगा।
मुजफ्फरपुर की लीची पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में 40 प्रतिशत लीची का उत्पादन भारत में होता है। यह आम की बहार आने से पहले गर्मियों की सौगात मानी जाती है। उत्तराखंड के कुछ इलाकों समेत प. बंगाल में भी इसकी फसल होती है परन्तु मुजफ्परपुर की लीची की रस की धार और सुगन्ध रसास्वादन को विशेष आनंद देती है। इस क्षेत्र की अधिकांश लीची निर्यात होती है जिससे किसानों को अच्छी आमदनी भी होती है। चमकी बुखार के साथ लीची का नाम जुड़ने से विदेश में तो इसका निर्यात घट ही गया है बल्कि भारत के दिल्ली और मुम्बई जैसे बड़े शहरों में भी नागरिक इसे खरीदने से डर रहे हैं।
श्री रूडी के अनुसार भारत के बाद चीन लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अतः इस नजरिये से भी विचार किया जाना जरूरी है हालांकि इसमें बहुत ज्यादा तर्क नजर नहीं आता है क्योंकि भारत के बाजारों में तो चीन के सेब से लेकर और न जाने क्या-क्या फल बिकते हैं। दूसरे मुजफ्परपुर में लीची सैकड़ों साल से हो रही है। बिहार के झंझारपुर में तो तुलसी की खेती भी जबर्दस्त होती है जिसका औषधीय प्रयोग होता है। इसी राज्य में ‘मखाने’ की पैदावार भी सबसे ज्यादा होती है। अतः मूल समस्या स्वास्थ्य क्षेत्र की बदहाली की है और बिहार में हालत यह है कि मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण सरकारी अस्पताल से कुछ दूरी पर ही ‘नरकंकालों’ का ढेर पड़ा हुआ मिला है जो लावारिस लाशों की अन्तिम क्रिया के बाद का है।
जाहिर है ये रवायतें इस राज्य में नई नहीं हैं और पिछले 15 वर्ष से माननीय नीतीश बाबू कमोबेश ही इस राज्य की बागडोर संभाले हुए हैं। यदि उनसे पहले लालू प्रसाद यादव के राज को ‘जंगल राज’ कहा जाता था तो इसे हम किस नाम से पुकारेंगे? इसके पीछे एक पूरा मनोविज्ञान है जो बिहार को लेकर पैदा किया गया है कि इस राज्य में ‘सब चलता है’। गर्मी से लेकर जाड़ा व बरसात की वजह से तो सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु इस राज्य में होती ही आयी है, अब पूरे देश के किसी भी अन्य राज्य में मानव निर्मित आपदा में भी सबसे ज्यादा संख्या में बिहारी ही मरते हैं। इसकी वजह यही है कि यहां के लोग रोजी-रोटी की तलाश में पूरे देश में फैले पड़े हैं। जाहिर है कि उनकी किस्मत में पिछले 15 वर्षों में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। कोई भी सामाजिक विज्ञानी पहली ही नजर में बता देगा कि ऐसे राज्य में सबसे ज्यादा जोर शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही दिया जाना चाहिए और दोनों ही क्षेत्राें में सार्वजनिक निवेश जमकर होना चाहिए परन्तु यह देश कहां जाकर माथा फोड़े जब सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.3 प्रतिशत ही स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है।
पाकिस्तान जैसे देश में इस मद में भारत से ज्यादा धन खर्च होता है। यही हाल शिक्षा का है। इन दोनों महत्वपूर्ण और बुनियादी विकास के दायरों को निजी क्षेत्र के भरोसे छोड़कर हम समावेशी विकास किसी हालत में नहीं कर सकते। पंचायत स्तर से लेकर नगर पालिका व जिला स्तर तक जब तक सरकारी स्वास्थ्य ढांचा मजबूत नहीं होगा तब तक सामान्य नागरिकों के स्वास्थ्य की गारंटी नहीं की जा सकती। इस सन्दर्भ में हमें वियतनाम जैसे छोटे से देश से सीखने की जरूरत है। वियतनाम में भी चमकी बुखार का प्रकोप चला था मगर उसने इसे काबू में कैसे कर लिया? यह क्षेत्र देशभर में रोजगार के नये अवसर खोलने की भी प्रचुर क्षमता रखता है।
जिला स्तर पर जब कोई बहुद्देश्यीय विशेषज्ञता का अस्पताल खुलता है तो बड़े-बड़े शहरों के अस्पतालों पर से दबाव कम होता है और रोगी को घर के नजदीक ही श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं लेकिन सबसे बड़ा भारतीय जनमानस मनोविज्ञान यह भी है कि सरकारी अस्पतालों के डाक्टर बहुत होशियार होते हैं क्योंकि उनका तजुर्बा बेजोड़ होता है। हमें भारत की जमीन की हकीकत के अनुसार ही अपनी वरीयताएं तय करनी होंगी। नीतीश बाबू से उम्मीद थी कि वह इस मोर्चे पर कुछ जमीनी काम करेंगे मगर वह भी हवा के रुख के साथ बह लिये और अब उल्टे मीडिया को ही डांट रहे हैं।