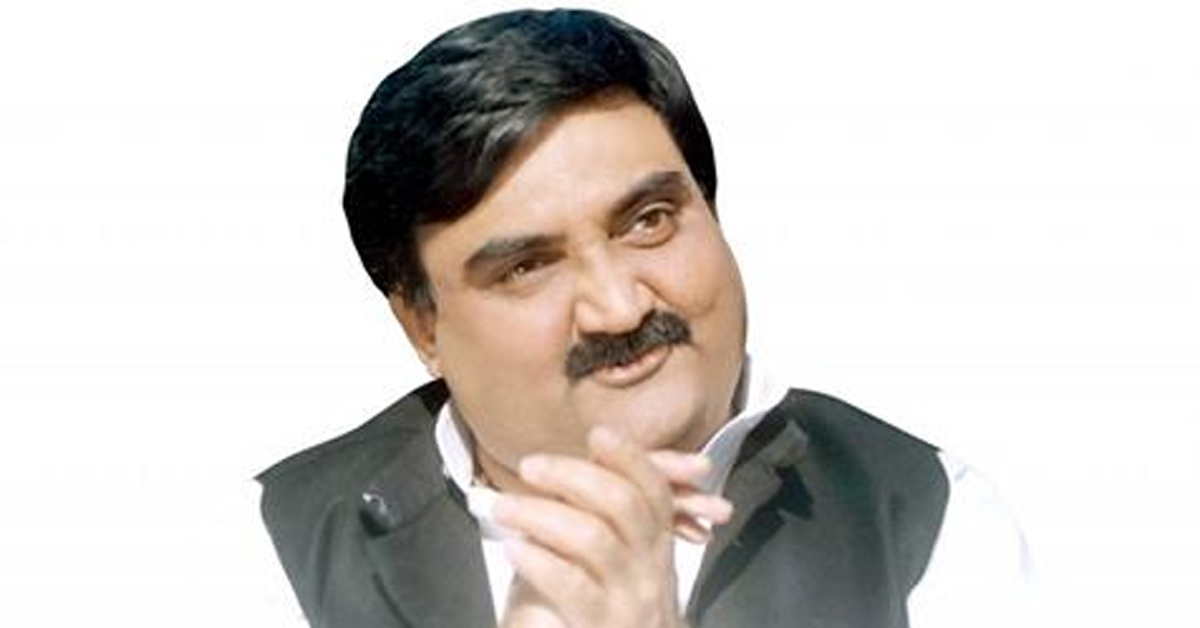भारत में चुनाव लगातार जिस तरह महंगे होते जा रहे हैं और इन पर जिस प्रकार विभिन्न राजनैतिक दल बेतहाशा धन प्रचार में लुटाते हैं, उसे देखते हुए लोकतन्त्र की आधारशिला में ही भ्रष्टाचार के बीज रोप दिये जाते हैं। अतः इस प्रक्रिया से जो भी फसल तैयार होगी वह भ्रष्टाचार को ही चौतरफा बिखेरेगी मगर इसके साथ एक और महत्वपूर्ण सवाल जुड़ा हुआ है कि राजनैतिक दलों को चुनावों मंे मनमाना खर्च करने की छूट देकर हमने प्रत्यक्ष रूप से सामान्य मतदाता को वोट का सौदा करने का तरीका तो ईजाद नहीं कर लिया है? इस व्यवस्था में जो पार्टी भी सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार पर खर्च करेगी वही अधिकाधिक मतदाताओं को प्रभावित करने में सक्षम हो सकेगी मगर इससे ही जुड़ा हुआ सवाल है कि राजनैतिक दलों के पास खर्च करने के लिए धन कहां से आयेगा? जाहिर है ये धन उन्हें बड़े-बड़े धन्ना सेठ और कम्पनियां ही देंगी। इस धन के बूते पर जब वे आम मतदाता के वोट लेंगी तो जो भी सरकार बनेगी वह इन धन्ना सेठों के उपकारों के तले दबी हुई होगी और ये धन्ना सेठ सत्ता में बैठे उन लोगों पर खर्च किये गये अपने धन की वसूली के रास्ते निकालेंगे।
अतः मूल सवाल यह है कि लोकतन्त्र में उस जनता का राज किस प्रकार काबिज होगा जिसके वोट से सरकारों का गठन होता है? शायद यही सब देखते हुए सत्तर के दशक मंे भाजपा के शर्षस्थ नेता डा. मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कि ‘वोट हमारा-राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।’ हकीकत यह है कि 1974 में जब स्व. जयप्रकाश नारायण ने अपना कथित सम्पूर्ण क्रान्ति आन्दोलन चलाया था तो उसका मुख्य केन्द्र चुनाव प्रणाली में सुधार ही था जिससे सामान्य बुद्धिमान व राजनीतिक रूप से सजग व्यक्ति भी चुनाव में खड़ा होकर लोकतन्त्र को ज्यादा से ज्यादा से जनाभिमुख बना सके और राजनैतिक दल भी प्रत्याशियों का चयन करते समय उसके धन बल की जगह पार्टी के सिद्धान्तों के प्रति उसके समर्पण को मुख्य योग्यता आधार बना सकें। इसकी असली वजह यह थी कि 1974 में राजधानी दिल्ली की सदर सीट पर 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में विजयी कांग्रेस प्रत्याशी स्व. अमरनाथ चावला जनसंघ के प्रत्याशी स्व. कंवर लाल गुप्ता के विरुद्ध विजयी हुए थे और उनके चुनाव को श्री गुप्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी थी।
इसका आधार चुनावों मंे सीमा से अधिक धन खर्च करना था। श्री चावला का चुनाव उच्च न्यायालय ने इसी आधार पर रद्द कर दिया था। इस पर तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने चुनावों से सम्बन्धित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 मंे संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया था कि किसी भी प्रत्याशी के चुनाव मंे राजनैतिक दल या प्रत्याशी का मित्र या समर्थक संगठन कितना भी खर्च कर सकता है। यह खर्च प्रत्याशी की निजी खर्च सीमा में नहीं आयेगा अर्थात पार्टी खर्च और प्रत्याशी खर्च को अलग-अलग कर दिया गया। इसके बाद चुनावों में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित खर्च सीमा बेमानी सी हो गई और चुनाव लगातार महंगे होते चले गये। आज हालत यह हो गई है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने पर खर्च एक सौ करोड़ तक को पार करने लगा है जाहिर है यह धन पार्टियां अथवा मित्र संगठनों द्वारा ही खर्च किया जाता है। जाहिर तौर पर यह धन पार्टियों को चन्दा देने वाले धन्ना सेठों या कम्पनियों का ही होता है। चुनाव के दौरान सत्ता पर काबिज किसी भी सरकार के मन्त्री सरकारी खर्चे पर चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। उनके दौरों का खर्च पार्टी ही उठाती है लेकिन हम देखते हैं कि प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं से लेकर सरकारी मन्त्रियों के चुनावी दौरों पर धन पानी की तरह बहाया जाता है।
चार्टर्ड हवाई जहाज उनकी सेवा में लगे रहते हैं। हजारों करोड़ रुपये खर्च किये जाते हैं। यहां तक कि रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए थैलियों के मुंह खोल दिये जाते हैं। दिहाड़ी पर लोगों को जमा किया जाता है मगर यह सब वही पार्टी कर सकती है जिसके पास पर्याप्त धन होता है। राजनैतिक दल हर साल अपने चन्दे का हिसाब आयकर विभाग में जमा करते हैं परन्तु इसका खुलासा आम जनता में नहीं करते। चुनावी बांड से यह काम और सरल हो गया है क्योंकि बांड खरीदने वाले का नाम बैंक गुप्त रखेंगे मगर सबसे ज्यादा जुल्म यह हुआ है कि विदेशी कम्पनियों की परिभाषा इस तरह गोलमोल और गुपचुप तरीके से संसद के माध्यम से ही बदल दी गई कि ये कम्पनियां भी चुनावी चन्दा देकर भारत की लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को सीधे-सीधे प्रभावित करेंगी। हम यह एेसा खतरनाक काम कर बैठे हैं जिसके लिए आने वाली पीढि़यां हमें कभी माफ नहीं करेंगी परन्तु राजनैतिक दलों को अब अपनी नाकामियों और लापरवाहियों का थोड़ा बहुत इल्म होने लगा है जिसकी वजह से चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को बुलाई गई बैठक में लगभग इन सभी ने इस बात की पुरजोर वकालत की कि पार्टियों द्वारा चुनावी खर्च करने की सीमा तय होनी चाहिए। इस बैठक के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने राय व्यक्त की कि यदि वर्तमान कानूनों के तहत एेसा करना संभव हुआ तो वह इस पर गौर करेंगे।
दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त के पाले में गेंद फेंक कर राजनैतिक पार्टियां अपने दायित्व से छुटकारा नहीं पा सकतीं क्योंकि आयोग संसद द्वारा बनाये गये कानूनों से बन्धा हुआ है। विदेशी कम्पनियों के चन्दे के मामले को तो संसद ने अलादीन के चिराग की तरह बजट प्रस्तावों में रख कर इस तरह कानून बना दिया कि इस पर राज्यसभा में नुक्ताचीनी भी नहीं हो सकती थी क्योंकि मनी बिल का मामला था मगर इससे यह तो सिद्ध होता है कि यदि राजनैतिक इच्छा शक्ति हो तो चुनावों से भी भ्रष्टाचार को समूल समाप्त किया जा सकता है और वैसा ही रास्ता निकाला जा सकता है जैसा विदेशी कम्पनियों के चन्दे के मामले में निकाला था मगर सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? क्योंकि सभी राजनैतिक दलों की गाड़ियां मोटे-मोटे चन्दे पर ही चलती हैं। हम कालाधन सारे संसार में ढूंढते फिरते हैं और अपना ही घर इस कालेधन के आगे गिरवी रखने में भी गुरेज नहीं करते? राजनैतिक दलों का चन्दा कर मुक्त होता है मगर उससे जो सरकारें बनती हैं वे लोगों से कर वसूल कर ही चलती हैं। हमने यह व्यवस्था राजनैतिक प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से बनाई थी जिससे लोकतन्त्र लगातार जीवन्त रह सके और हर वैध राजनैतिक विचारधारा को फलने-फूलने का अवसर मिल सके मगर इसका रूपान्तरण जिस तरह ‘धनतन्त्र’ में हो रहा है वह लोकतन्त्र में आम आदमी की भागीदारी लगातार सीमित करता जा रहा है। अब तो टैक्नोलोजी ने इतना विकास कर लिया है कि चुनाव प्रचार यदि हम चाहें तो न्यूनतम धन खर्च करके भी कर सकते हैं। मैं चुनाव सुधारों की विभिन्न समितियों और आयोगों की रिपोर्टों की चर्चा इसीलिए नहीं कर रहा हूं कि तब प्रचार व सूचना टैक्नोलोजी का उन्नयन नहीं हुआ था।