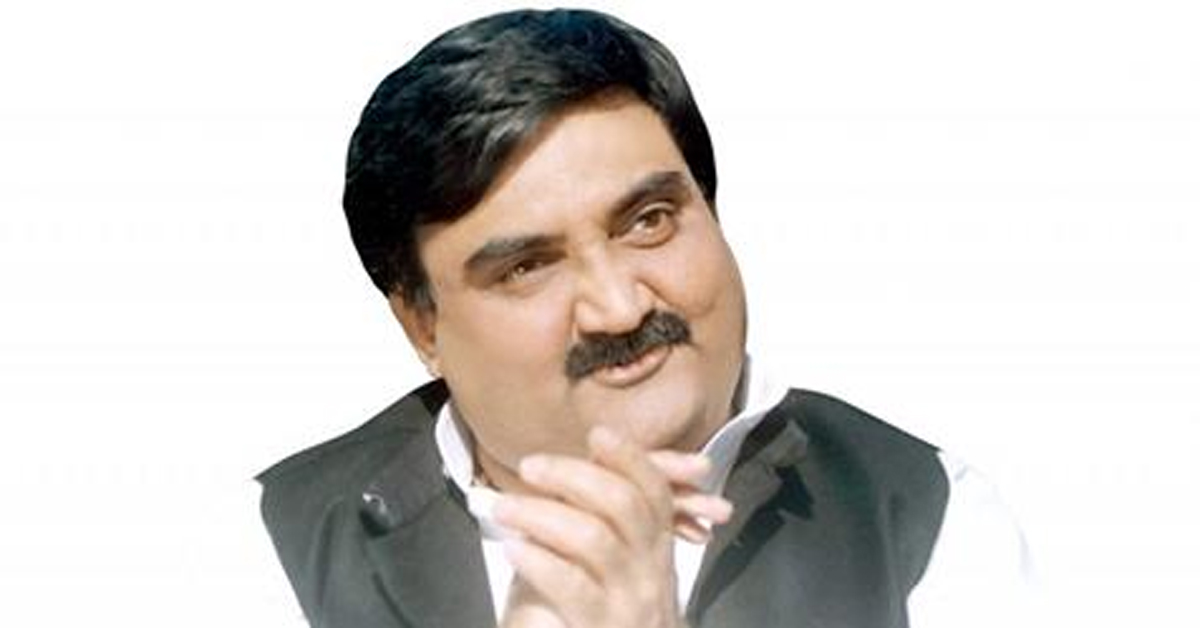मौसम ने पिछले कुछ वर्षों से हमें चौंकाने का जो सिलसिला शुरू किया है, वह अभी भी कायम है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि वैसे तो हमारे लिए मुसीबत के रूप में आती धमकाती ही रही है लेकिन बारिश का बदलता चक्र अब परेशानी ला रहा है। कभी बेमौसम बरसात ने किसानों को तबाह किया तो कभी बरसात नहीं होने से किसान तबाह हुआ। फसल की बर्बादी होने पर किसानों की आत्महत्याओं की खबरें पहले भी आती थीं और आज भी आ रही हैं। अब महाराष्ट्र में सूखे का संकट पैदा हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 931 और गांवों के सूखा प्रभावित होने की घोषणा की है।
इससे पहले केन्द्र सरकार ने घोषणा की थी कि अक्तूबर में महाराष्ट्र की 358 तहसीलों में से 151 सूखा प्रभावित हैं। पानी के लिए तरसते किसान अब पलायन करने लगे हैं। चारों तरफ भूख, बेबसी और लाचारी है। देश को शानदार सियासी चेहरे देने वाले महाराष्ट्र में किसानों के मुद्दे फिर सवाल बने हैं। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल हो रहा है। सतारा जिला के मान तालुका के 1400 परिवार अपने पशुओं को लेकर निकटवर्ती महासवाड़ा में पहुंच चुके हैं आैर उन्होंने अपने पशुओं को बचाने के लिए एक शिविर स्थापित किया है। इस शिविर में 7 हजार के करीब पशु हैं। जब तक वर्षा नहीं आती तब तक वह वापस अपने तालुका में नहीं लौटेंगे।
पिछले दो वर्षों से किसानों की फसल तबाह हो चुकी है। बेरोजगार किसान मजदूरी के लिए गुजरात के शहरों में जा चुके हैं। सूखा प्रभावित गांवों को टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है लेकिन यह पानी भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इन लोगों के लिए अपने पशु बचाना बहुत जरूरी है। इन्हें पानी भी चाहिए और चारा भी। भगवान का शुक्र है कि महासवाड़ा में पानी है क्योंकि राजेवाड़ी बांध में पानी है। स्थानीय पालिका पानी भी मुहैया करा रही है और शिविर में पशु चिकित्सक भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। समाजसेवी संस्थाएं भी लोगों की मदद कर रही हैं। महाराष्ट्र की तरह कर्नाटक के कई जिलों में सूखे का संकट है लेकिन वहां के हालात इतने भयानक नहीं हुए। देश के 125 करोड़ लोगों के पेट भरने की जिम्मेदारी इन्द्रदेव के ऊपर है। ‘भारत की कृषि मानसून पर आधारित है’ यह जुमला लोगों के अंतःकरण में रच-बस गया है। कभी हमने इससे उबरने की कोशिश ही नहीं की। आखिर आजादी के 70 वर्षों बाद भी हमारी खेती को क्यों मानसून के भरोसे रहने पड़ता है? क्यों नहीं अब तक सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की जा सकी? क्यों नहीं अब तक फसलों की ऐसी प्रजातियां अमल में आ सकीं जिन्हें उपजाने में नाममात्र पानी की जरूरत पड़े?
कारण कुछ भी रहे हों, पिस रहा है अन्नदाता। ऐसे में परम्परागत रूप से की जा रही खेती को आधुनिकता का पुट दिए जाने की जरूरत महसूस हो रही है लेकिन राज्य सरकारें किसानों को 100-200 रुपए के मुआवजे के चैक बांटकर किसानों के कर्जे माफ करके वाहवाही लूटती नजर आ रही है। पहले तो महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से ही सूखे की खबरें आती थीं अब तो सूखा कई अन्य क्षेत्रों में फैल गया है। फसल बीमा योजना का भी किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बीमा कम्पनियां किसानों से पंजीकरण शुल्क तो वसूल रही हैं लेकिन उन्हें बीमा देने में कई तरह की बहानेबाजी करती हैं। किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं का भाषण कृषि आैर किसान से शुरू होकर उन्हीं पर खत्म होता है लेकिन सत्ता में आने के बाद सचिवालय में बैठकर उनके लिए सही नीति बनाने की बात आती है तो वह सब कुछ भूल जाते हैं। जब तक किसान को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जाता तब तक कर्जमाफी का कोई फायदा नहीं होने वाला।
निराशाजनक पहलू इस बात के लिए मजबूर करता है कि मानसून की कमी से कृषि को बचाया कैसे जाए? वर्षों से एकपक्षीय सिंचाई नीति मानसून के फेल होने की दशा में कृषि को बचाने में नाकाम रही है। परम्परागत सिंचाई तंत्र तालाब, पोखर और झीलों आदि की कृषि के विकास में भूमिका रही है। यह कम कीमत के स्रोत हैं। यहां तक कि कमजोर मानसून की स्थिति में भी इनको आसानी से भरा जा सकता है। जहां 1950 के दशक में इनका हिस्सा 19 प्रतिशत था, अब घटकर 3 प्रतिशत रह गया है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि वृहद सिंचाई प्रणाली कमजोर मानसून की स्थिति में बेहद उपयोगी नहीं है। देश में वृहद सिंचाई प्रणाली या लघु जल निकायों में केन्द्र की बेहतर व्यवस्था है, उसका जवाब देना मुश्किल है। दोनों ही कई मामलों में एक-दूसरे की पूरक हैं। दक्षिण भारत में वृहद नहर प्रणाली से कई तालाब भी सम्बद्ध हैं।
लघु जल योजनाओं को नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इनसे 70 फीसदी छोटे किसानों की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। जरूरत है नई नीतियां बनाने कीं। अब ऐसी प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं जो सूखे की स्थिति में भी अच्छी उपज दे सकती हैं। धान की ऐसी प्रजाति विकसित हो चुकी हैं जो 100 से 105 दिनों में तैयार हो जाती हैं और पानी का इस्तेमाल कम होता है। हमें कम पानी से तैयार होने वाली सब्जी, फल की प्रजातियों को अपनाना होगा। संकट की घड़ी में बांध और नहर बहुत उपयोगी नहीं हैं। यदि हम जल भंडारण का उचित प्रबन्धन कर लें तो समस्या हल हो जाएगी। हम वर्तमान रणनीति में बदलाव कर संकट से निजात पा सकते हैं। बार-बार किसान ऋण माफ करने की बजाय हमें इस धन का इस्तेमाल जल भंडारण के लिए करना चाहिए।